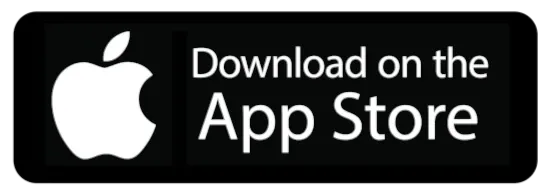ग्रामीण भारत: कैसे बदलेगी तस्वीर?
शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऊर्जा, ईंधन समेत समस्त सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ हों

गांवों से शहरों की ओर पलायन के मुख्यत: दो कारण होते हैं- शिक्षा और रोजगार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में 'इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023' को संबोधित करते हुए देश के विकास से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिन पर काम करने की जरूरत है। खासतौर से शहरों पर दबाव घटाने के लिए गांवों तक उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का उल्लेख किया जाना अत्यंत प्रासंगिक है।
आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऊर्जा, ईंधन समेत समस्त सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ हों। साथ ही वहां रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन किया जाए। गांवों से शहरों की ओर पलायन के मुख्यत: दो कारण होते हैं- शिक्षा और रोजगार।यदि प्रारंभिक शिक्षा गांवों में और उच्च शिक्षा निकटवर्ती क्षेत्रों में ही उपलब्ध करा दी जाए तो निश्चित रूप से बड़े शहरों से आबादी का दबाव कम हो सकता है। कई शहर तो ऐसे हैं, जहां छोटे-से कमरे में छह से ज्यादा विद्यार्थियों को रहना पड़ता है। वे बड़े सख्त हालात में गुजारा करते हुए सुनहरे भविष्य के सपने संजोते रहते हैं। कई कोचिंग संस्थानों के पास पर्याप्त स्थान नहीं होता। ऐसे में एक ही कक्ष में क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी बैठाए जाते हैं।
नौकरियों के मामले में भी कुछ ये ही हालात हैं। शहरों में निजी क्षेत्र में कार्यरत एक औसत कर्मचारी को अपने वेतन का बड़ा हिस्सा मकान किराए और दफ्तर आने-जाने पर खर्च करना पड़ता है। उसके बाद परिवार की जरूरतें मुश्किल से पूरी होती हैं। अगर कोई बीमार हो जाए और अस्पताल में डॉक्टर की फीस, जांच और दवाइयों पर मोटा खर्चा हो जाए तो घर का बजट बिगड़ जाता है।
अगर सरकारों ने गंभीरता दिखाते हुए कुछ ऐसे इंतजाम किए होते, जिससे शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा समेत जरूरी सुविधाएं बेहतर ढंग से गांवों में उपलब्ध करा दी जातीं तो आज शहरों पर इतना दबाव नहीं होता। महानगरों में तो हालत यह है कि सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए किराए पर मकान लेना बहुत बड़ी चुनौती है।
महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जो दर्शन दिया, उससे ग्रामीण स्वावलंबन को अलग नहीं किया जा सकता। विडंबना है कि गांधी के देश में गांवों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना कि देना चाहिए था। कई गांव तो ऐसे हैं, जिनमें दशकों तक बिजली नहीं पहुंची। लोग केरोसीन की चिमनी जलाकर उसे ही अपना भाग्य स्वीकार कर चुके थे।
सरकारी स्कूल, अस्पताल और आम लोगों के काम से जुड़े दफ्तरों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं पहुंचीं और न ही इनके प्रबंधन में कोई खास सुधार किए गए। लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए शहर जाना पड़ता, जिसमें कई बार एक दिन से ज्यादा समय लग जाता था। आज इंटरनेट से कई काम काफी आसान हो गए हैं, लेकिन सुधारों की गुंजाइश है।
इस धारणा को बदलना होगा कि रोजगार का अर्थ सिर्फ 'सरकारी नौकरी' है। हमें खेती-किसानी को मुनाफे का धंधा बनाना होगा। इसके लिए इजराइल के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिसने बंजर व सूखी धरती को उपजाऊ बनाकर विश्व को चकित कर दिया। खाद्यान्न व दलहन के अलावा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा का विस्तार होगा।
जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया, बड़े उद्योग, कारखाने, शॉपिंग मॉल का संचालन अवरुद्ध हो गया, तब खेती ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी और अर्थव्यवस्था को संभाला था। निस्संदेह देश के विकास के लिए बड़े उद्योगों और कारखानों की जरूरत होती है, लेकिन गांव व खेती के महत्त्व को कम नहीं आंकना चाहिए।
राष्ट्रपति के भाषण के इन शब्दों की ओर नीति निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए, जिनके अनुसार, वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी 40 करोड़ के मौजूदा स्तर से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक होने का अनुमान जताया गया है।
इसका यह अर्थ है कि करीब ढाई दशक बाद 50 प्रतिशत से ज्यादा देशवासी शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। क्या हमारे शहर इसके लिए तैयार हैं? इसको ध्यान में रखते हुए अभी से धरातल पर ठोस काम करने होंगे। गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विस्तार करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। जिस दिन ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर होगा, बापू का एक सपना पूरा हो जाएगा।